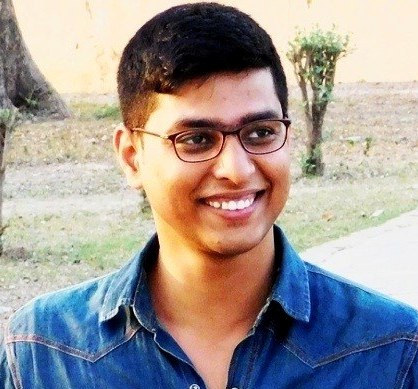
लेनिन मौदूदी (Lenin Maududi)
हम सबको ये समझने का वक्त आ गया है कि हर समाज के केंद्र में इसकी राजनीति होती है. अगर राजनीति घटिया दर्जे की होगी तो सामाजिक हालात के बढ़िया होने की उम्मीद करना बेमानी है. भारत में सेक्युलर योद्धा दावा कर रहे हो हैं कि वे फासीवाद से लड़ रहे हैं इसलिए ये हर उस व्यक्ति को अपने साथ मिला लेना चाहते हैं जो संघी-फासीवाद के खिलाफ है. ऐसा करते हुए वे मुस्लिम साम्प्रदायिक संगठनो को भी अपने साथ मिला लेते हैं. सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि एक बड़े खतरे, बड़ी बुराई के लिए छोटे खतरे या छोटी बुराई को नज़र अंदाज़ कर दें. एक तर्क ये भी दिया जाता है कि फासीवाद और साम्प्रदायिकता में हमे चुनना हो तो हम साम्प्रदायिकता को चुनेंगे. ऐसा तर्क देने वाले मानसिक रूप से अपंग हो चुके हैं. उन्हें समझ में नहीं आता कि हर अच्छी दिखने वाली चीज़ ज़रूरी नहीं कि सही ही हो. हमें अच्छे (Good) और सही (right) में से हमेशा सही की ओर जाना चाहिए. ऐसे ही मानसिक रूप से कुछ अपंग बुद्धिजीवी लोगों ने आपातकाल के दौरान राजनीतिक रूप से अछूत RSS को मौका दिया कि वो भारत के राजनीतिक पटल पे अपनी पहचान बना ले। उस वक़्त बड़ा अच्छा लग रहा था कि कैसे सभी विचारधारा एक छत्री के नीचे आ गई? इंदिरा गाँधी को हरा दिया, वाह वाह!
गाँधी जी की गाय समझे जाने वाले मुसलमानों ने पहली बार कांग्रेस का साथ छोड़ा और इंदिरा गाँधी के खिलाफ वोट किया और इस हद तक गए कि आरएसएस के लोगो को भी वोट किया. नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गाँधी पूरी तरह से हार गई. पर सवाल ये है कि आखिर जीता कौन? हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कोई भी साम्प्रदायिक/फासीवादी ताकतें जनभावना को आधार बना कर आसानी से लोकतंत्र में अपनी पैठ बना लेती हैं और फिर ये इसी लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती हैं.
हम आज उसी आपातकाल की गलतियों को भुगत रहें है जो उस वक़्त के बुद्धिजीवियों और राजनीतिक नेताओं ने की थी. आज फिर हम वही गलती कर रहें हैं. फासीवाद से लड़ने के नाम पर मुस्लिम साम्प्रदायिक संगठनों को ये सेक्युलर योद्धा मौका दे रहे हैं. अभी बहुत अच्छा लग रहा है, सब सही नज़र आ रहा है और हमें इस बात की कोई परवाह नही कि हम मुस्लिम युवाओं को इन मुस्लिम साम्प्रदायिक संगठनों के चंगुल फसा रहे हैं. ज़्यादातर मुस्लिम लड़के तो इन चर्चित सेक्युलर योद्धाओं (liberal- Communist) के चेहरों के चक्कर मे ही इनसे जुड़ रहे हैं कि जब इतने बड़े लोग इनके साथ हैं तो ये संगठन सही ही होंगे.
अक्सर ये देखा जाता है कि ये सेक्युलर योद्धा हिन्दू साम्प्रदायिकता पर तो मुखर होते हैं पर मुस्लिम साम्प्रदायिकता पर चुप्पी साध लेते हैं. ऐसा कर के वो मुस्लिम समाज पर कोई अहसान नहीं कर रहे बल्कि इस तरह वो हिन्दू साम्प्रदायिकता को बढावा दे रहे हैं. ये बात मुस्लिम समाज को भी समझने की ज़रूरत है कि अल्पसंख्यक साम्प्रदायिकता, बहुसंख्यक साम्प्रदायिकता से नहीं लड़ सकती. जब एक गुंडा (मुख़्तार अंसारी) आपका शेर होगा तो बहुसंख्यक का शेर तुम्हारे शेर से कम क्यों हो? जब ओवैसी मुस्लिम एकता का नारा देगा और मुस्लिम होने के नाते वोट करने की बात करेगा तो संघी हिन्दू होने के नाते एक होने और वोट करने की बात क्यों न करें? क्या ये कहना गलत होगा कि जज़्बाती मुद्दों की सियासत में सबसे पहले उस मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व को रखा जा सकता है जिसका बड़ा हिस्सा कुलीन यानी अशरफ वर्ग के मुसलमानों में से आता है. क्या ये कहना गलत है कि ओवैसी, आज़म खान जैसे नेता हमेशा भावनात्मक मुद्दों पर मुखर रहते है और गरीब विरोधी राजनीतिक तंत्र की संरचना पर कभी कोई आवाज नहीं उठाते.
आज अंसारी समाज (जुलाहों) की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है GST बुनकरों/ जुलाहों की कमर तोड़ने को तैयार है. क्या ये हमारे मुस्लिम नेतृत्व के लिए मुद्दा है? कुरैशी (कसाई) समाज लगातार प्रताड़ित हो रहा है पर हमारा मुस्लिम नेतृत्व ‘तीन तलाक‘ के मुद्दे पर हर सड़को पर निकलेगा क्यूंकि इस समाज का नेतृत्व जिनके हाथो में है वह मुस्लिम समाज के आर्थिक-सामाजिक रूप से सम्पन्न जातीय पृष्ठभूमि से आते हैं. ये न मुसलमानों के पसमांदा समाज को जानते हैं और न उसकी परेशानियों को और अगर जानते भी है तो उसपे बात नहीं करना चाहते क्यूंकि ऐसा कर के वो मुस्लिम समाज की एकरूपता की छवि को तोड़ देंगे.
इसीलिए यह कुछ सांकेतिक और जज्बाती मुद्दों जैसे बाबरी मस्जिद, उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पर्सनल लॉ इत्यादि, को उठाती रहते हैं. जिस पर सेक्युलर , लिबरल और कम्युनिस्ट बुद्धिजीवी इनके साथ नज़र आते हैं. इन मुद्दों पर गोलबंदी करके और अपने पीछे मुसलमानों का हुजूम दिखा कि मुसलमानों की अगड़ी बिरादरियां और उनके दबदबे में चलने वाले संगठन (जमीअत-ए-उलेमा-ए-हिन्द, जमात-ए-इस्लामी, आल इण्डिया पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरात, पॉपुलर फ्रण्ट ऑफ इण्डिया इत्यादि) अपना हित साधते रह कर सत्ता में अपनी जगह पक्की करते रहे हैं. वही सेक्युलर, लिबरल और कम्युनिस्ट बुद्धिजीवी भी इनका साथ दे के अल्पसंख्यक समाज में अपनी पहुँच बढ़ाते हैं ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा फण्ड मिल सके. इस सेक्युलर योद्धाओं को हिन्दू दलित नज़र आते हैं पर मुस्लिम दलित नज़र नहीं आते. इन बुद्धिजीवियों के पेट में मरोड़ हो जाता है पसमांदा शब्द सुनते ही. पर जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने पसमांदा शब्द का प्रयोग किया सेक्युलर योद्धाओं के हल्के में हाहाकार मच गया पासमांदा समाज के नेता इनको भाजपा के एजेंट नज़र आने लगे. पसमांदा समाज के नेताओ के खिलाफ गोलबंदी कर ली गई और उन पर व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए गए. इनके साथ पसमांदा तबके के कुछ व्यक्तियों जिनका ‘अशराफिकरण’ हो चुका है (और जो अगड़े मुसलमानों की मानसिक गुलामी करते हैं और उस पर फख्र करते हैं), को आगे रखा गया लेकिन किसी नेकनियती से नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के अंदरूनी जातपात के तजाद को काबू में रखने के लिए.
यहाँ एक बात और समझने की है कि भारत में ‘सेक्युलरिज़्म‘ का अर्थ ‘मुस्लिम तुष्टीकरण’ के रूप में किया जाता है. भाजपा आसानी से ये बात हिंदू मतदाताओं को समझा पा रही है. बड़ी बात ये है कि हिन्दू मतदाता इस अर्थ को खारिज नहीं कर रहे. अगर भाजपा के हिंदू बहुसंख्यकवाद से अन्य पार्टियों का अल्पसंख्यक सेक्युलरवाद टकराएगा, तो इस मुकाबले में जीतने वाले का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है. इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सेक्युलरिज़्म की नई व्याख्या जाति/वर्ग की एकता के आधार पर हो जहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकवाद का कोई स्थान न बचे. एक ओर हिन्दू-मुस्लिम दलित-पिछड़ों तो दूसरी ओर हिन्दू-मुस्लिम अगड़ों की सियासत एकता भारत में एक नई राजनीति का आगाज़ करेगा. पसमांदा आन्दोलन इस ठोस हकीक़त पर टिका हुआ है कि जाति भारत की समाजी बनावट की बुनियाद है. इसलिए सामाजिक-राजनीतिक विमर्श जाति को केन्द्र में रखकर ही किया जा सकता है. हम मानते हैं कि किसी एक जाति की इतनी संख्या नहीं है कि वह अपने आप को बहुसंख्यक कह सके. जब कोई बहुसंख्यक ही नहीं तो फिर अल्पसंख्यक का कोई मायने नहीं रह जाता. जातियों/वर्गो के बिच एकता ही एक मात्र उपाय है भारतीय समाज के हिन्दुकरण या इस्लामीकरण को रोकने का.
~~~
लेनिन मौदूदी लेखक हैं. पसमांदा नज़रिये से समाज को देखते-समझते-परखते हैं और अपने लेखन में दर्ज करते हैं.
Magbo Marketplace New Invite System
- Discover the new invite system for Magbo Marketplace with advanced functionality and section access.
- Get your hands on the latest invitation codes including (8ZKX3KTXLK), (XZPZJWVYY0), and (4DO9PEC66T)
- Explore the newly opened “SEO-links” section and purchase a backlink for just $0.1.
- Enjoy the benefits of the updated and reusable invitation codes for Magbo Marketplace.
- magbo Invite codes: 8ZKX3KTXLK