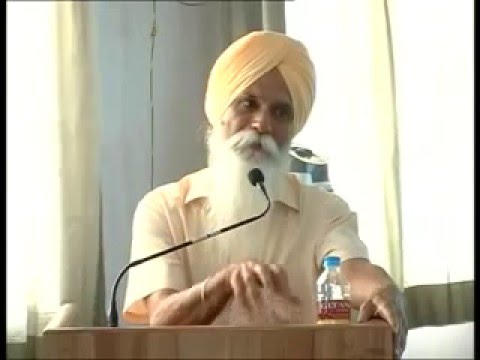
सरदार अजमेर सिंह (S. Ajmer Singh)
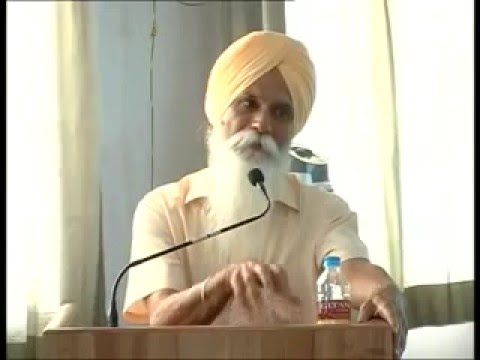 ‘कौमवाद’ का संकल्प, मूल रूप में एक पश्चिमी संकल्प है जो अपनी साफ़ साफ़ सूरत के साथ मध्ययुग के आखिरी दौर में प्रकट हुआ. यह प्रिक्रिया जितनी व्यापक यानी फैली हुई है, उतनी ही अलग भी है. व्यापकता, एतिहासिकता और भिन्नता-विभिन्नता इसके संयुक्त लक्षण हैं. इसलिए इसकी कोई ठोस या पक्की परिभाषा संभव नहीं. कौमवाद ने इतिहास के अलग अलग पड़ावों में अलग अलग रूप धारण किया. शायद इसी वजह के चलते ही, इसको अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरह से समझा जाता है. आम तौर पर, इससे भाव, अपनी कौम और देश के प्रति पूरण वफादारी से लिया जाता है. इस भाव को दो पक्षों से ठीक नहीं माना जा सकता. एक तो ‘कौम’ (नेशन) और ‘देश’ (कंट्री) एक ही चीज़ नहीं, दो अलग अलग श्रेणियां हैं. एक देश में कई कौमें हो सकती हैं, या एक ही कौम कई देशों में बंटी-बिखरी हो सकती है. दूसरा, कौमवाद अपने विशाल अर्थों में किसी आदर्श के प्रति मोहब्बत और भक्ति का अभ्यास है. यह मोहब्बत मिटटी के साथ हो सकती है, धर्म, सभ्याचार और भाषा के साथ हो सकती है. यूरोप में चली विशेष एतिहासिक प्रिक्रिया ने सदियों से अलग अलग और ख़ास भूगोलिक जगहों पर इकट्ठे रहते आ रहे लोगों को एक कर दिया था. दरअसल इस प्रिक्रिया ने ही अलग अलग समूहों में रहते लोगों को इतिहास, विरासत, भाषा, सभ्याचार और मानसिक शक्ल की सामूहिक सांझ जैसे निखरे हुए राष्ट्रवाद के लक्षण प्रदान किये थे. बल्कि मध्ययुग के अंत तक आते आते उन्हें अपने अपने स्वतंत्र कौमी राज्यों का वरदान भी नसीब हो गया. इस तरह अपने कौमी राज्य के प्रति श्रद्धा और वफादारी का प्रबल जज़्बा, उन यूरोपिए-कौमों की ठोस पहचान बन गया.
‘कौमवाद’ का संकल्प, मूल रूप में एक पश्चिमी संकल्प है जो अपनी साफ़ साफ़ सूरत के साथ मध्ययुग के आखिरी दौर में प्रकट हुआ. यह प्रिक्रिया जितनी व्यापक यानी फैली हुई है, उतनी ही अलग भी है. व्यापकता, एतिहासिकता और भिन्नता-विभिन्नता इसके संयुक्त लक्षण हैं. इसलिए इसकी कोई ठोस या पक्की परिभाषा संभव नहीं. कौमवाद ने इतिहास के अलग अलग पड़ावों में अलग अलग रूप धारण किया. शायद इसी वजह के चलते ही, इसको अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरह से समझा जाता है. आम तौर पर, इससे भाव, अपनी कौम और देश के प्रति पूरण वफादारी से लिया जाता है. इस भाव को दो पक्षों से ठीक नहीं माना जा सकता. एक तो ‘कौम’ (नेशन) और ‘देश’ (कंट्री) एक ही चीज़ नहीं, दो अलग अलग श्रेणियां हैं. एक देश में कई कौमें हो सकती हैं, या एक ही कौम कई देशों में बंटी-बिखरी हो सकती है. दूसरा, कौमवाद अपने विशाल अर्थों में किसी आदर्श के प्रति मोहब्बत और भक्ति का अभ्यास है. यह मोहब्बत मिटटी के साथ हो सकती है, धर्म, सभ्याचार और भाषा के साथ हो सकती है. यूरोप में चली विशेष एतिहासिक प्रिक्रिया ने सदियों से अलग अलग और ख़ास भूगोलिक जगहों पर इकट्ठे रहते आ रहे लोगों को एक कर दिया था. दरअसल इस प्रिक्रिया ने ही अलग अलग समूहों में रहते लोगों को इतिहास, विरासत, भाषा, सभ्याचार और मानसिक शक्ल की सामूहिक सांझ जैसे निखरे हुए राष्ट्रवाद के लक्षण प्रदान किये थे. बल्कि मध्ययुग के अंत तक आते आते उन्हें अपने अपने स्वतंत्र कौमी राज्यों का वरदान भी नसीब हो गया. इस तरह अपने कौमी राज्य के प्रति श्रद्धा और वफादारी का प्रबल जज़्बा, उन यूरोपिए-कौमों की ठोस पहचान बन गया.
पश्चिम की यह हकीक़त पूरब का सपना था. इस सपने ने पूरब के अलग अलग ईलाकों में अलग अलग स्वरूप धारण किये. भारत में हिन्दू वर्ग के, पश्चिमी विद्या और विचारों से प्रभावित पढ़े लिखे तत्वों को, इस सपने ने ख़ास तौर पर आकर्षित किया. इसकी वजह यह थी कि यह सपना उनको भारत पर काबिज़ होकर राज करने के सीधे-सपाट राह की और इशारा करता था. यदि समूचा भारत युरोपिये-कौमी-राज्यों की तरह ही एक जुट राष्ट्रवाद का स्वरूप अपनाता था तब पश्चिमी लोकतंत्र के कायदे कानूनों के अनुसार हिन्दू बहुगिनती वर्ग ही भारतीय राजभाग का प्राकृतिक दावेदार बनता था. सो इसी सोच और प्रेरणा के तहत हिन्दू वर्ग ‘भारतीय राष्ट्रवाद’ का एक दृढ़ झंडाबरदार बनके आगे आया और साथ ही पश्चिम की नई लोकतान्त्रिक विचारधारा का भी. ऐसा इसलिए था क्यूंकि यहाँ के हिन्दू को जिस तरह से कौमवाद अच्छा लगता था उसी तरह यूरोप के कत्लों की गिनती पर आधारित लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली भी इसके वर्गीय हितों को घी की तरह लगती थी.
हिन्दू लीडरों की और से जोशोखरोश से अपनाई गई इस ‘कौमप्रसती’ का असली मामला आखिर है क्या? यह बात उनकी कथनी और करनी से भलीभांति स्पष्ट हो जाती है. लाला लाजपत राय का यह पक्का मानना था कि “प्राचीन भारत के गौरव की गाथा में से ही भारतीय लोगों में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति गौरव की भावनाएं पैदा हो सकती हैं और उनमें देश प्रेम और कौमप्रस्ती (राष्ट्रवाद) का जज़्बा उभर सकता है.” लाला जी का यह कथन उनकी आत्मकथा (स्टोरी ऑफ़ माय लाइफ) से लिया गया है, जिसमें वह यह बात भी कहते हैं कि ‘ब्रह्मों समाज’ का अग्रदूत बाबु नवीन चंदर राय, “हिंदी को भारत की कौमी (राष्ट्रीय) भाषा के तौर पर देखता था और चाहता था कि यह भारतीय कौमियत (राष्ट्रवाद) के चबूतरे (यानि मंच) की आधारशिला बने. इन विचारों ने मुझे बड़े ठोस रूप से प्रभावित किया…. मेरे चरित्र पर सब से गाढ़ा असर हिंदी एजिटेशन (1882-83) ने डाला. इसमें मेरे भीतर कौमी भावनाएं जागृत हुईं. जब मैं लाहौर में पढ़ता था मेरा यह मानना था कि अंग्रेजों ने हमें मुसलामानों के ज़ुल्मों से मुक्ति दिलाई है…. तब आर्य समाज की जो एक छोटी-सी कश्ती थी, मेरे लिए हिन्दू कौमियत की नाव थी वो.”
लाला लाजपत राय का यह पक्का मानना था कि “प्राचीन भारत के गौरव की गाथा में से ही भारतीय लोगों में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति गौरव की भावनाएं पैदा हो सकती हैं और उनमें देश प्रेम और कौमप्रस्ती (राष्ट्रवाद) का जज़्बा उभर सकता है.” लाला जी का यह कथन उनकी आत्मकथा (स्टोरी ऑफ़ माय लाइफ) से लिया गया है, जिसमें वह यह बात भी कहते हैं कि ‘ब्रह्मों समाज’ का अग्रदूत बाबु नवीन चंदर राय, “हिंदी को भारत की कौमी (राष्ट्रीय) भाषा के तौर पर देखता था और चाहता था कि यह भारतीय कौमियत (राष्ट्रवाद) के चबूतरे (यानि मंच) की आधारशिला बने. इन विचारों ने मुझे बड़े ठोस रूप से प्रभावित किया…. मेरे चरित्र पर सब से गाढ़ा असर हिंदी एजिटेशन (1882-83) ने डाला. इसमें मेरे भीतर कौमी भावनाएं जागृत हुईं. जब मैं लाहौर में पढ़ता था मेरा यह मानना था कि अंग्रेजों ने हमें मुसलामानों के ज़ुल्मों से मुक्ति दिलाई है…. तब आर्य समाज की जो एक छोटी-सी कश्ती थी, मेरे लिए हिन्दू कौमियत की नाव थी वो.”
अरबिंदो घोष भारत के दोबारा निर्माण के लिए वेदों और भगवत गीता की शिक्षाओं को आधार बनाने के विचार की खुल्लम-खुल्ली वकालत करता था. प्रसिद्द इतिहासकार आर.सी.मजूमदार के मुताबिक बंगाल में ही ‘नेशनल सोसाइटी’ नाम की एक ‘कौमप्रस्त’ सभा के अग्रदूत नाबागोपाल मित्र का मानना था कि “भारत में कौमी एकता (राष्ट्रीय एकता) की बुनियाद हिन्दू धर्म है.” बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में हिन्दू जनता को उभारने के लिए गणेश और शिवजी के नाम पर मेले और उत्सव आयोजित करने की परंपरा शुरू की. उसने खुलेआम यह मांग की कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए क्यूंकि “यह हिन्दू राष्ट्रवाद के लिए एक ज़रूरी जोड़ने वाली कड़ी है.” इसी दौरान बिहार में उर्दू को “विदेशी ज़ुबान” कह कर उसकी भर्त्सना करने और पाबंदी लगाने की आवाजें उठानी शुरू हो गईं. गाँधी, जो कि खुद सनातनी हिन्दू थे, भारतीय लोगों में कौमपरस्ती की भावनाएं पैदा करने के लिए धार्मिक मुहावरे की बहुत अहमियत देखता था. इसी लिए वह राजनीति के क्षेत्र में हिन्दू चिन्हों का खुलकर इस्तेमाल करता था. ‘स्वैराज’ पर ‘राम राज्य’ जैसे संकल्प उस की इसी धरना की पैदाइश थीं. और तो और, सेकुलरिज्म का ‘दूत’ समझे जाते जवाहर लाल नेहरु जैसे नवीन आभास वाले लीडर भी अपने हिंदूवादी झुकावों से मुक्त नहीं थे. नेहरु अपनी आत्मकथा में इस बात को कुछ यूं स्वीकार करता है : “मेरे पीछे, कहीं नीम चेतना में, ब्राह्मणों की सैंकड़ों पुश्तों की नस्ली यादें पड़ी हैं. मैं जातिवाद की इस विरासत से या ऐसी किसी सोच से बेपरवाह नहीं हो सकता. यह दोनों मेरे वजूद का हिस्सा हैं…..”
अरबिंदो घोष भारत के दोबारा निर्माण के लिए वेदों और भगवत गीता की शिक्षाओं को आधार बनाने के विचार की खुल्लम-खुल्ली वकालत करता था. प्रसिद्द इतिहासकार आर.सी.मजूमदार के मुताबिक बंगाल में ही ‘नेशनल सोसाइटी’ नाम की एक ‘कौमप्रस्त’ सभा के अग्रदूत नाबागोपाल मित्र का मानना था कि “भारत में कौमी एकता (राष्ट्रीय एकता) की बुनियाद हिन्दू धर्म है.” बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में हिन्दू जनता को उभारने के लिए गणेश और शिवजी के नाम पर मेले और उत्सव आयोजित करने की परंपरा शुरू की. उसने खुलेआम यह मांग की कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए क्यूंकि “यह हिन्दू राष्ट्रवाद के लिए एक ज़रूरी जोड़ने वाली कड़ी है.”
हिन्दू लीडरों के इस विचारधारक तरीके ने भारत में इस्लामी भाईचारे में अपने धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हितों को महफूज़ करने का तुरंत और तीखा सरोकार पैदा किया. बौद्धिक मुस्लिम वर्ग ने अपने भाईचारे के हितों की रक्षा के लिए माकूल रणनीति घड़ने के काम को पूरी शिद्दत और गंभीरता से हाथ में ले लिया. इस बात को मुस्लिम वर्ग की संप्रदायवाद रूचियों का नाम दिया गया. देश भर में लोगों, खास तौर पर हिन्दुओं में मुस्लिम विरोधी भावनाएं पैदा हो गईं. यह मुस्लिम विरोधी विश्वास अभी तक ज्यों के त्यों कायम है. सिर्फ हिन्दू जनता में ही नहीं, उसी हद तक ही सिखों में भी हैं. इस की बुनियादी विचारधारक वजह ‘भारतीय राष्ट्र’ और ‘राष्ट्रवाद’ के बारे में मन में बनीं (दरअसल गहरे धसीं हुईं) गलत धारणाएं हैं. हिन्दू कांग्रसी लीडरों की तरफ से ‘भारती कौम’ का संकल्प उभारा जा रहा था, उसका हकीक़त में और तर्कयुक्त आधार नहीं था. पश्चिम में जो कौमें एक इकहरे रूप में संगठित हुईं, वह महज़ लीडरों की नेक ईच्छाओं के चलते नहीं थीं हो गईं. एक लम्बे एतिहासिक अमल में उनकी सचमुच की संयुक्त कौमी हस्ती विकसित हो चुकी थी. इसलिए वहां कौमी जज़्बे ने सभी जज़्बात (धार्मिक, नस्लीय आदि) पर फतह हासिल कर हो चुकी थी.
लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में मामला ऐसा नहीं था. पहली बात, यदि मूल भारतीय सभ्याचार और परम्परा को ही लें तब इस में नस्लीय, धार्मिक, भाषा से जुड़े, और सभ्याचारक पक्ष से इतने विरोध और विभिन्नताएं हैं कि Ainslie T. Embree नाम के प्रसिद्ध बरतानवी चिंतक (जिसने भारतीय धार्मिक और सभ्याचारक परम्परा के विषय पर गाढ़ा और गहन गंभीर अध्यन किया है) का यह मानना है कि “किसी और जगह, यह अलग अलग कौमियतें होनी थीं, जैसे कि यूरोप में हुआ.” [अर्थात अगर भारत की भिन्नताएं भारत की जगह कहीं और होतीं तो ये अलग अलग कौमियतें यानि राष्ट्र होने थे – अनुवादक] हिंदुस्तान में इस्लामी सभ्यता की आमद कोई साधारण घटना नहीं थी. इस ने भारत के सामाजिक सभ्याचारक जीवन में एक बिलकुल ही नई स्थिति पैदा कर दी थी. यह दो धर्मों के बीच भिन्नता का मामला नहीं रह गया था. यह दो संस्कृतियों की आमने सामने की टक्कर थी जिसने भारत का सभ्याचारक जोग्रफिया ही बदल के रख दिया था. यह सही है कि सदियों के लम्बे सह-वास ने इन दोनों धर्मों, संस्कृतियों और धार्मिक भाईचारों में विरोध और टकरावों के साथ साथ आपसी मेलजोल का सांझें भी पैदा कीं. पर इसके बावजूद दोनों का मुकम्मल मिलाप कभी संभव नहीं हुआ. दोनों साथ साथ रहते हुए भी एक दुसरे में अभेद नहीं हुए. मेक्सिको के नोबल इनाम से नवाज़े शायर और प्रतिभाशील चिन्तक ओक्टावियो पाज़ ने इस प्रक्रिया को अपनी अनोखी शैली में इस तरह ब्यान किया है :
“सदियों तक साथ साथ रहते हुए भी दोनों भाईचारों ने अपनी अपनी पहचान बरकरार रखी हैं. दोनों का मुकम्मल मिलाप नहीं हुआ. फिर भी उनको कई चीज़ें आपस में जोड़ती हैं, जैसे कि संगीत, लोक कला, पहरावा और इतिहास. एक ऐसा इतिहास, जो उनको जोड़ता भी और फाड़ता भी है. वह इकट्ठे ज़रूर रहते रहे परन्तु उनका सह-वास प्रतिस्पर्धात्मिक, शक, धमकियों और मूक नाराज़गियों, जो अक्सर ही खून ख़राबों में लिप्त होती रही है, से भरपूर रहा है.” भारत की समाजिक सभ्याचारक हकीक़त के बारे में Ainslie T. Embree के यह विचार भी काफी भावपूर्ण हैं कि “यदि उन्नीसवीं सदी के बरतानवी और फ़्रांसिसी टकसाली मॉडल के मापदंड अपनाये जाएँ तब भारत कौमवाद (यानि राष्ट्रवाद) की कोई भी शर्त पूरी नहीं करता. क्यूंकि एक सांझी भाषा, साँझा गौरवमई एतिहासिक अनुभव, एक सांझी धार्मिक परंपरा और नस्लीय एकरूपता जैसी सभी चीज़ों की भारत में खटकती-हुई गैरहाज़री है. उसपर, यहाँ हिन्दू बहुगिनती के दरम्यान एक बड़ी मुस्लिम अल्पसंख्यक अस्तित्व गहरे विभाजनों का सबब बना हुआ है. उन दोनों धर्मों की परम-सच की कल्पना इतनी अलग अलग है कि कोई असाध्य आशावादी ही, इन्हें स्वै-सजग (अपनी पहचान के प्रति जागृत) भाईचारों के सहभाव की कल्पना कर सकता है.”
यदि उन्नीसवीं सदी के बरतानवी और फ़्रांसिसी पारंपरिक मॉडल के मापदंड अपनाये जाएँ तब भारत कौमवाद (यानि राष्ट्रवाद) की कोई भी शर्त पूरी नहीं करता – Ainslie T. Embree
यह बात नहीं कि भारत में अलग अलग धार्मिक फिरकों में आपसी प्रेम और भाईचारे की बिलकुल ही कोई संभावना नहीं. या फिर ऐसा लक्ष्य या आशा करनी ही फ़िज़ूल है. इतिहास में इन समुदायों के बीच आपसी नफरत और बैर-विरोध की खाईयों को भरने के काफी शलाघायोग प्रयास हुए हैं. कितने ही धार्मिक सुधारकों, गुरुओं, अवतारों, पीरों-पैगंबरों और भगतों और सूफियों ने मानवीय प्यार और भाईचारे का संदेस फ़ैलाने के कल्याणकारी जतन किए हैं. इनके पीछे किसी समुदाय को नीचा दिखाने या किसी की धार्मिक सभ्याचारक पहचान को चोट लगाने की मंदभावना नहीं थी. यह ‘मानस की जाति सभै एकै पहचानबो’ [सभी मनुष्यों की जाति सिर्फ एक ही है, मानव – अनुवादक] की सच्ची और साफ़ भावना थी जिसमें किसी मैल, फरेब या छल के लिए कोई जगह नहीं थी. मानव एकता के यह यत्न बिलकुल ही निष्क्रिय साबित हुए, ऐसा नहीं कहा जा सकता. इतिहास में कई मौके आये जहाँ अलग अलग समुदायों में विरोध और कड़वाहट की भावनाएं मद्धम पड़ीं और मानवीय भाईचारे की ज्योति प्रज्वलित हुई. सिकंदर लोधी, शेरशाह सूरी और अकबर जैसे बादशाहों ने भी इस दिशा में ईमानदार यत्न जुटाए. इससे अलग अलग सभ्यचारों ने एक दूजे का प्रभाव तो ज़रूर कबूल किया परन्तु इनमें पूरण मिलाप कभी नहीं हुआ. ज्यादा से ज्यादा, सामयिक एकता और राजनीतिक गठजोड़ों के दौर ज़रूर आये. ऐसे अस्थायी और आंशिक अमल सांझी कौमियत के विकास के लिए काफी नहीं होते. इसलिए जिसे ‘भारतीय कौमप्रस्ती’ कहा जा रहा है, वह तत्व रूप में हिन्दू कौमियत [यानि हिन्दू राष्ट्रवाद] के निर्माण का प्रोजेक्ट ही था. इसलिए मुस्लिम भाईचारे में जागरूक तत्वों की और से, इसे अपनी धार्मिक और सभ्याचारक पहचान के लिए गंभीर खतरे के तौर पर देखना बेवजह नहीं था. उनको महसूस होते खतरे और सरोकार बेवजह नहीं थे.
हिन्दुवाद की इस चढ़ाई के जवाब में ही, मुस्लिम वर्ग में, स्वैरक्षा के लिए, मुस्लिम कौमप्रस्ती जज़्बा प्रबल हुआ जिसको कि हिन्दू लीडरों ने मुस्लिम ‘कट्टरता’ और ‘फिरकापरस्ती’ कहकर इसकी भर्त्सना करना शुरू कर दिया. यदि हिन्दू मुस्लिम संबंधों के मसले को इस सन्दर्भ में रखकर नहीं देखा जाता और कोंग्रेस की अगुवाई तले आज़ादी की लहर के हिंदूवादी तत्व को लगातार ध्यान में नहीं रखा जाता तो मुस्लिम भाईचारे के भय, जज़्बात और मांगों को सही तौर पर समझ पाना बिलकुल ही संभव नहीं. ज़्यादातर मुस्लिम लीडर, पहले पहल, ‘मुस्लिम अलगाववाद’ की विचारधारा के साथ सिर्फ सहमती नहीं थी बल्कि वह इसके निंदक भी थे. यह कांग्रेस पार्टी और इसके लीडरों को धकेल के मुस्लिम अलगाववाद की पटरी पर चढ़ाया. उदहारण के तौर पर, सर सय्यद अहमद खान, पहले, पश्चिमी प्रभावों के चलते, ‘भारतीय कौमप्रस्ती’ की धरना और भावना के कायल थे. धार्मिक भेदभाव को साइड में रखके, सभी भारतीय लोगों की एकता और भलाई उस का आदर्श था [या सही शब्दों में केवल हिन्दू मुस्लिम में अभिजात्य वर्ग की एकता – अनुवादक].
लेकिन जब उसको लगा कि भारत में ‘नुमाईंदा सरकार का एक अर्थ यह है कि यह अल्पसंख्यक, अर्थात मुसलमानों पर बहुगिनती, अर्थात हिन्दू वर्ग का राज’ होगा, तब उसका भारतीय कौमवाद से पूरी तरह मोह भंग हो गया और कांग्रेस पार्टी की स्थापना से जल्दी ही बाद वह मुस्लिम कौमप्रस्ती का बेबाक प्रवक्ता बन गया. इसी तरह, आगा खां जब केन्द्रीय परिषद् के मेम्बर (1902 से 1904 तक) थे तब वह गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक उस्ताद मान कर चलता था और अलग चुनाव क्षेत्रों का कट्टर विरोधी था. लेकिन दो सालों में ही उसका कांग्रेसी लीडरों से इस कद्र मोह भंग हुआ कि वह मुस्लिम लीग का अग्रदूत हो चला. आगा खां के ही बताने के मुताबिक मुहम्मद अली जिनाह, पहले पहल मुस्लिम लीग का कट्टर विरोधी हुआ करता था. उसका यह मानना था कि अलग चुनाव क्षेत्र का सिद्धांत ‘भारतीय कौम’ को आपस में बांटने का काम करता है. इसलिए, वह, तकरीबन बीस पच्चीस साल मुस्लिम लीग की तीखी आलोचना करता रहा. यह नेहरु रिपोर्ट (1928) थी जिसने जिन्नाह जिन्ना के लिए कांग्रेसी लीडरों के चेहरों से ‘कौमप्रस्ती’ का भ्रमिक पर्दा उतार फेंका और उनके असली फिर्काप्रस्त चेहरे के इरादे साफ़ उजागर हो गए. एक बार कांग्रेसी लीडरों के असली किरदार को बूझ लेने के बाद, जिन्ना ने फिर से इस मामले में कोई टपला नहीं खाया. इसके बाद उसको कांग्रेसी लीडरों के किसी भी झांसे में आने से कोरा इनकार कर दिया और ठोस तज़ुर्बे से ग्रहण की इस विद्या का आखरी सांस तक पल्ला नहीं छोड़ा.
~~~
सरदार अजमेर सिंह पंजाब के एक जाने माने इतिहासकार हैं। उन्होंने सिख दृष्टिकोण से ब्राह्मणवाद की निशानदेही की और पंजाब के इतिहास को नई रौशनी में लिखा है.
गुरिंदर आज़ाद इस आलेख के अनुवादक हैं. वह राउंड टेबल इंडिया –हिंदी के एडिटर हैं.
Magbo Marketplace New Invite System
- Discover the new invite system for Magbo Marketplace with advanced functionality and section access.
- Get your hands on the latest invitation codes including (8ZKX3KTXLK), (XZPZJWVYY0), and (4DO9PEC66T)
- Explore the newly opened “SEO-links” section and purchase a backlink for just $0.1.
- Enjoy the benefits of the updated and reusable invitation codes for Magbo Marketplace.
- magbo Invite codes: 8ZKX3KTXLK