
झरना साहू (Jharna Sahu)
मैंने इस लेख को इसीलिए लिखना शुरू किया क्योंकि लिखने से हमें हमारे काम व् जीवन पर पुनर्विचार करने में काफी मदद मिलती है। अपने काम की परिस्थितियों व् एक टीचर बने रहने के संघर्ष के कारण, हम कुछ टीचर जो रायपुर के औद्योगिक इलाके के एक छोटे से प्राइमेरी स्कूल में पढ़ाते हैं, ने इस सवाल पर मिलकर विचार करना शुरु किया कि एक टीचर का उत्थान कैसे होता है? इस सवाल के जवाब को खोजने की कोशिश के लिए हमने अपने आसपास के कम फीस वाले (low fee) प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स के काम को लेकर एक शोध किया। शोध के डेटा (data) से हमें कई चौंकाने वाली चीज़ें देखने को मिलीं। स्कूलों में टीचर्स के साथ मैनेजमेंट का कैसा व्यवहार होता है? इसका असर उस टीचर की पूरी आत्मछवि पर कैसे पड़ता है? उनके काम के ऊपर कैसे पड़ता है? इन्हीं सब सवालों से जूझते हुए हम अपने काम के ऊपर पुनर्विचार करने पर मजबूर हो जाते हैं। साथ में, हमें इस सवाल का भी सामना करना पड़ता है कि सच में एक टीचर आखिर कौन-कौन से काम करता/करती है और समाज में उनकी जगह क्या है? यह लेख शायद इन सभी टीचर्स को खुद से पूछने का एक प्रयास है।
अगर देखा जाए तो जितने भी लोअ-फी (low fee) यानि कम फीस वाले प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ ज़्यादातर पढ़ाने वालीं महिलाएँ बहुजन हैं। स्कूलों में उनके साथ काफी शोषण होता है। उनकी मेहनत के अनुसार ना ही सम्मान मिलता है, ना ही वेतन, और ना ही अपनी बातों को कह पाने की जगह। मुझे उम्मीद है कि इस लेख को पढ़ने के बाद टीचर्स को अपने ऊपर हो रहे शोषण का भी एक आभास हो सकेगा जिससे हम संगठित होकर अपने हकों की माँग कर सकेंगे। साथ ही, वे इस लेख को पढ़कर अपने काम व जीवन के ऊपर पुनर्विचार कर पाएँगे और उनमें अपने काम को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने काम का सही सम्मान कर सकेंगे।
एक बहुजन टीचर को टीचर बनने या बने रहने के लिए उसके आसपास की सामाजिक ताकतों के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो परिवार में ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब कोई अध्यापन के काम में जाता है तो शुरू में परिवार वाले बहुत खुश रहते हैं कि उनके घर की लड़की पढ़ाने जा रही है, कि वो एक ‘मैडम’ बन गई है। मगर अध्यापन के काम में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसका अंदाज़ा उनको नहीं होता है। असल में उनके काम को काम के नज़रिए से देखा ही कहाँ जाता है? उल्टा हममें से कईयों को यह बोला जाता हैं कि ‘ये तो पढ़ायेल बस जाथे’ यानि कि ‘ये तो बस पढ़ाने जाती है’। जब सैलरी की बात आती हैं, तब कहा जाता है कि ‘बहुत कम है… बढ़ाने को क्यों नहीं बोलते?’ ऐसी बातों को सुनकर हमारा भी हौसला कई बार टूट जाता था। यह भी एक कारण है जिससे एक टीचर बने रहना मुश्किल हो जाता है।
मगर मुश्किल केवल परिवार तक ही सीमित नहीं होती। जातिगत माहौल में झेलने वाली सामाजिक चुनौतियाँ ढेर सारी होती हैं। कहा जाता है व माना जाता है कि स्कूल में शिक्षिकाएँ सुरक्षित रहती हैं मगर ऐसा नहीं है। स्कूल के अंदर व स्कूल के बाहर उनके आसपास के माहौल के कारण वे अक्सर सुरक्षित नहीं होती हैं। यह असुरक्षा खासकर हमें हमारी जाति व लैंगिकता (gender) के कारण होती है।
हमारे साथ हुई कुछ घटनाएँ शायद इन बातों पर रोशनी डाल सकती हैं। स्कूल में पढ़ाने का काम मैंने 2016 में शुरू किया। मुझे इस काम (शिक्षिका का) के बारे में अपनी एक सहेली के द्वारा पता चला। उस समय हम कॉलेज में पढ़ते थे। मैंने अध्यापन शुरू किया तो हमें दोनों तरफ मैनेज करना पड़ता था। दिक्कत तो होती थी लेकिन अन्य पढ़ाने वालों का सपोर्ट भी था तो यह काम ठीक लगने लगा। उस समय जिस परिस्थिति में हम थे, हमने सोचा नहीं था कि हम बहुजन (बहुजन से यहाँ तात्पर्य है जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी के श्रेणी में गिने जाते हैं) एक साल से ज्यादा इस स्कूल में टिक पाएँगे। एक ओर खुद की पढ़ाई पर ध्यान देने का मन भी था और दबाव भी। दूसरी ओर इस स्कूल में पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होने के कारण शुरू में लगता था कि हम शायद ही इस नई पद्धति को अपना पाएँगे। लेकिन धीरे-धीरे यह समझ आया कि एक तरह से, यहीं, स्कूल में हमारी पढ़ाई भी हो रही थी और हमें कई चीज़ें सीखने को मिल रहीं थीं जो कभी खुद की स्कूली पढ़ाई में समझ ही नहीं आई थीं।

यह स्कूल एक मज़दूर संगठन का स्कूल है जिसे बस्ती के लोगों ने ढाई दशक से अधिक समय हुआ, मिलकर स्थापित किया। असल में मेरी सहेली और मैं भी इसी स्कूल से पढ़कर निकले थे। लेकिन जिस समय हम यहाँ पढ़ते थे तब होमवर्क और पाठ्यक्रम को याद कराने पर ही ज्यादा जोर दिया जाता था। एक रटन-पद्धति में ही पढ़ाई होती थी जैसे अभी भी अधिकतर स्कूलों में होता है।
लेकिन जब हम यहाँ पढ़ाने आए तो तरीका बदल चुका था। अब इस स्कूल के टीचर्स बाकी स्कूलों की तरह छत्तीसगढ़ पाठयपुस्तक से पढ़ाने व रटने–रटाने वाली शिक्षा नहीं देते हैं। बच्चों को इस स्कूल में पढ़ने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि पढ़ाई उनके जीवन से भी जुड़ी है और उनके लिए अर्थपूर्ण भी है। दुसरे स्कूलों में देखें तो गणित नाम से ही ज़्यादातर बच्चे डर जाते हैं। लेकिन इस स्कूल में ज़्यादातर बच्चों का सबसे पसंदीदा विषय ही गणित है। बच्चों के लिए गणित केवल कुछ अमूर्त संख्याओं का विषय नहीं है। यहाँ के बच्चे संख्याओं की दुनिया में वास्तव में जीते हैं। साथ में, स्कूल में हम यह भी प्रयास करते हैं कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा के बजाय एक आपसी सम्मान और जुड़ाव के साथ काम करने का कल्चर हो। हम उनको एक ऐसी शिक्षा देने की कल्पना करते हैं जहाँ बच्चे सोचने–समझने, आत्मविश्वासी, निडर, अपने और दूसरों के हको की माँग रखने वाले इंसान बने।
आज के महौल में पौराणिक कथाओं (भगवत गीता, रामायण, महाभारत आदि) को पाठ्यक्रम में लाने की कोशिश की जा रही है। आजकल ‘हिंदू राष्ट्र’ की बात को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी भी हमारे जातिगत समाज में भेदभाव होता है। हिंदू राष्ट्र में तो जातिगत ताकतें और भी बढ़ेंगी। मगर जिस तरीके से लोगों के अंदर हिंदू धर्म को सबसे अच्छा मानने का माहौल बनाया जा रहा उससे यह बात लोगों को दिख नहीं रही है। इसीलिए उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले भी कम है। ऐसे माहौल में हम संविधान के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमारा जो काम है वह समाज को थोड़ा टक्कर देने वाला है। इसके चलते हम आसानी से समाज के ‘रक्षकों’ के टारगेट में आ जाते हैं और ऐसे ही हमारे काम और हमारे टीचर्स के चरित्र के ऊपर कई बार सवाल उठता है।
एक ऐसी घटना तब हुई थी जब बस्ती में गणेश की मूर्ति बिठाई गई थी। स्कूल के बच्चे वहाँ जाते तो पंडाल के लड़के बच्चों के माथे पर टीका लगाते। एक दिन स्कूल के कुछ मुस्लिम बच्चों के मना करने के बावजूद भी उनके ऊपर टीका लगाने की कोशिश की गई थी। यह सब देखकर हमने बच्चों को टीका लगाकर आने से मना किया। उसके अगले दिन जब बच्चे गणेश पंडाल के पास गए और वहाँ के आर.एस.एस. व बजरंग दल के लड़के बच्चों के माथे पर टीका लगाने लगे तो बच्चों ने टीका लगवाने से मना किया और कहा कि मैडम ने कहा है किसी को भी टीका नहीं लगाना है। इसी बात से वे लड़के काफी चिढ़ गए और अगले दिन ही 20 से 25 लोग स्कूल में आए और इसी बात पर दो टीचर्स के साथ बदतमीजी व गाली-गलौज करने लगे। उसमें से कुछ लड़कों ने वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया ग्रुप में डाल दिया। कई बार पहले भी इन लड़कों से टीचर्स को धार्मिक काम में शामिल होने के लिए बोला गया है, मगर टीचर्स ऐसे कामों में शामिल नहीं हुए हैं। जब हम मानव अधिकार के हनन के खिलाफ आवाज़ उठाने सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो फिर इन्ही लड़कों ने हमें आतंकवादी, नक्सलवादी, आदि बुलाया।
जब से हमारा वेतन बढ़ा, तब से टीचर्स को पैसों की खातिर बिकने वाला बोल-बोलकर उनका जीना हराम कर रखे थे ये लोग। टीका कांड के बाद तो हमारे हर काम पर नज़र रखने लगे और बच्चों को भी यह कहकर भड़काने लगे थे कि तुम्हारे स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं होती इत्यादि। कुछ टीचर्स (टीचर्स/शिक्षिकाओं) को बीच बस्ती में घेरकर भीड़ इकट्ठा करके सवाल-जवाब करना, उनके पहनावे व सोच व विचारधारा पर उँगली उठाना, टीचर्स के साथ बैठक बुलाकर उसमें दारू पीकर आना और अपने हाथ को नीचे करते हुए कहना कि एक टीचर को टीचर की तरह रहना चाहिए, यानि नीचे रहना चाहिए। स्कूल को आने जाने वाले रास्ते पर ताना व धमकी देना, हमारे साथ इन लड़कों ने यह सब किया। साथ में बस्ती के वरिष्ठ मुखिया लोगों ने भी उन्हीं के साथ खड़े होकर कई बार हमारे काम पर सवाल उठाया। जब भी कोई सामाजिक पारम्परिक व धार्मिक कामों से हटकर बदलाव का काम करते हैं तो हमें इस जातिगत समाज से लगातार जूझना पड़ता है। खासकर के जब बदलाव लाने वाली महिलाएँ होती हैं, तब उनको और अधिक, अलग-अलग तरीके अपनाकर पीछे धकेलने की कोशिश की जाती है ताकि वे दबकर रहें।
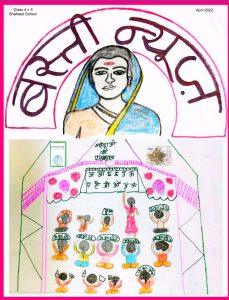
‘बस्ती न्यूज़’ पत्रिका के लिए बच्चों द्वारा बनाया एक चित्र
इन सब घटनाओं के चलते बस्ती वालों के मन में केवल यह बात बैठ गई है कि हम लोग समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं। किसी ने देखा-समझा नहीं कि हम बच्चों को पढ़ाने में कितनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए कितना सोच रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। वैसे भी कई लोगों के मन में धारणा होती है कि बच्चों को पढ़ाने का काम आसान काम होता है। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और हम एक महिला हैं तो बच्चों को तो संभालना हमारा कर्तव्य है ही! लोगों की नज़र में बच्चों को पढ़ाने का मतलब अक्सर यही होता है कि पुस्तक से वाक्यों को पढ़ाना और उनको कॉपी में लिखवाना। सच्चाई तो इस से बहुत दूर है। एक टीचर के हाथ में बच्चों का पूरा भविष्य रहता है जिसको बनाने में टीचर को अपना पूरा योगदान देना पड़ता है। अपने काम को बेहतर करने के लिए पहले से ही योजना बनानी पड़ती है। मगर योजना बनाना और सीखना भी एक ज्ञान औेर दक्षता की बात होती है कि हम बच्चों की जरूरत के अनुसार क्या और किस विधि से किसी विषय को पढ़ाएँ ताकि सभी बच्चों में उस अवधारणा की पकड़ बन सके और उनकी सोचने-समझने की क्षमता में विकास हो सके। यह सब करने के लिए एक टीचर को अपने काम के बारे में लगातार पुनर्विचार करना पड़ता है ताकि वह अपने काम को और बेहतर कर पाए। वो स्कूल तक ही सीमित नहीं रह सकती। बच्चों को पढ़ाने के अलावा वो उनको इमोशनली (भावनात्मक) भी सपोर्ट करती है। मगर इन सब के बावजूद भी उनके काम का कोई खास सम्मान नहीं होता। अगर बच्चे कुछ गलती कर दें तो सारा का सारा दोष टीचर के ऊपर आता है कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें ऐसा ही सिखाया है क्या?
ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में यदि टीचर से अपने एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासनिक) काम में कुछ गलती हो जाए तो उनको मैनेजमेंट से भी काफी सुनना पड़ता है। स्कूल का काम घर ले जाए तो परिवारवालों से भी सुनना पड़ता है। इतना सब काम करने के बावजूद टीचर्स को बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पढ़ाने के काम को काम के रूप में माना ही नहीं जाता है और टीचर्स को काम करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाता। न्यूनतम वेतन से कई गुणा कम वेतन मिलने के बाद भी इसी वेतन में से हम कई टीचर्स अपने घर को चलाने के लिए काफी सहयोग करते हैं। शुरू में मुझे भी बहुत कम वेतन मिलता था तो मेरे घरवाले बोलते थे कि मुझे वेतन बढ़ाने की माँग करनी चाहिए। लेकिन संगठन का स्कूल होने के नाते स्कूल में भी उतना पैसा नहीं था तो हम भी किस हक से वेतन बढ़ाने की माँग रख सकते थे? बात यह भी थी कि जो हमारे सीनियर थे उनका भी वेतन काफी कम था और स्कूल में नियम था कि एक साल के बाद तो सबको बराबर वेतन मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से मजदूर संगठन की महिलाओ ने काफी लड़कर टीचर्स के वेतन को बढ़ाने के लिए संगठन में ही काफी संघर्ष किया। मेरे स्कूल आने से पहले एक समय ऐसा था जब एक पुरुष टीचर भी पढ़ाता था और उसको महिला टीचर्स के मुकाबले ज़्यादा वेतन दिया जाता था जबकि काम बराबर था। कुछ टीचर्स ने जब संगठन के महिला साथियों के साथ मिलकर इस असमानता पर सवाल किया तो यह कहा गया कि इस वेतन से कम में पुरुष आएँगे नहीं इसीलिए उनको ज़्यादा दे रहे हैं!
क्या यह भी महिलाओं को पीछे करने का एक और तरीका नहीं है? जैसे समाज में होता है उसी तर्क को यहाँ भी लाया जा रहा था जिस से महिलाओं व उनके काम को कम दर्जे पर ही देखा जा रहा था। महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर जोर देकर संगठन की महिला साथियों ने टीचर्स के वेतन को बढ़ाने का संघर्ष किया।
आज मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा कमाती हूँ। जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिलता लेकिन घर में मेरे आर्थिक सहयोग के चलते थोड़ी-बहुत आज़ादी तो बढ़ गई है। जब मैं इन सब के बारे में सोचती हूँ तो मन में यही ख्याल आता हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं के नेतृत्व को और खासकर बहुजन महिलाओं के नेतृत्व को बनने में रुकावटें डालती हैं। लेकिन इन संघर्षों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और साथ में हमें एक जगह भी मिली है जहाँ हम अपनी बातों को रख सकते हैं, एक साथ में सोच सकते हैं।
सबसे ज़्यादा ताकत तो हमें अपने साथियों से ही मिलती है। हमारी दोस्ती, आपसी सहयोग और एकता से। स्कूल में काम करने का जो माहौल बनाया गया है, टीम में जो साथीपना है, मेरे एक टीचर बने रहने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। हमें अपने काम में बहुत सहयोग मिलता हैं चाहे वो क्लास की योजना बनाने की बात हो, क्लास लेना हो, बच्चों को समझने-समझाने की बात हो या फिर गर्मी के दिनों में छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ से बाहर अलग अलग जगह पर जाकर वर्कशॉप में शामिल होने का मौका हो। इन सभी चीज़ों से मैं अपने शिक्षण के काम में खुद को काफी आगे बढ़ा महसूस करती हूँ। काम करने में मज़ा भी आता है। टीचिंग के अलावा भी हम वर्कशॉप और मीटिंग के दौरान अलग-अलग चिंतकों के विचारों को जानकार व् पढ़कर आपस में चर्चाएँ करते हैं। हमने बचपन में स्कूल में भी कई चिंतकों और नेताओं के बारे में पढ़ा। गांधी से लेकर राधाकृष्णन और तिलक तक। जिस तरह से हमें इन लोगों के बारे में पढ़ाया जाता था यह सब लोग हमसे बहुत दूर लगते थे। आज़ादी की कहानी भी ऐसे बोली जाती थी जैसे कि महात्मा गांधी ने अकेले ही इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद किया। लेकिन जब हम यहाँ वर्कशॉप और मीटिंग में बाबासाहेब आंबेडकर और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के विचारों व जीवनी को पढ़ने लगे तो ऐसा लगा कि हम अपने जीवन से भी जोड़कर उनके जीवन को देख सकते थे। इससे हमें अपनी स्कूली शिक्षा में अपनी जाति के कारण जिस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा है और उसका असर हमारे पूरे जीवन को कैसे प्रभावित करके रखता है, वो सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं। पहले तो मुझे संविधान के बारे में ठीक से पता नहीं था। उसके उद्देश्य, उसके अनुच्छेद या उसके मूल्यों से दूर-दूर तक कोई ठोस रिश्ता नहीं था हमारा। स्कूल में काम करते हुए संविधान के उद्देश्य और कई सारी चीज़ों के बारे में जानने व सीखने को मिला जिन्होंने मेरे व्यक्तित्व को काफी प्रभावित किया। बाबासाहेब और पेरियार के विचारों में बहुत तर्क दिखा जिससे मुझे भी अपने जीवन के बारे में सोचने का मौका मिलने लगा। इन सब से मेरी खुद की सोच बदली और विकसित हुई। जहाँ एक तरफ हमारी सोच में कई बदलाव आने लगे वहीं दूसरी तरफ हमारे काम से हमारे बच्चों के मन भी नए सपने पनपने लगे।
उन्हीं में से कुछ बच्चे अभी टीचर बनना चाहते हैं ताकि वो भी बड़े होकर एक अच्छी व अर्थपूर्ण शिक्षा देने के साथ-साथ अलग-अलग जगह जाकर लोगों से मिलें, घूमें और चीज़ों के बारे में और सीख सकें। लेकिन यह बदलाव का रास्ता सीधा और आसान नहीं। इसके लिए कई लड़ाईयाँ लड़नी पड़ी हैं चाहे वह घर में हों, मोहल्ले में हों या खुद से भी क्यों न हों। जब मैंने शुरू में अध्यापन का सोचा तो वेतन एक मुख्य कारण था। मैं कमाना चाहती थी ताकि में अपनी शिक्षा का खर्च उठा पाऊँ। और मेरी समझ में पढ़ाना सिर्फ पढ़ाना था और ऐसा कई लड़कियाँ कॉलेज का फीस जमा करने के लिए करती थीं ना कि एक सीखे जाने वाला काम समझती थीं। मगर, अब यह सोच पूरी तरह से बदल गई है। कॉलेज को कंप्लीट किए कई साल हो गए मगर मैं आज भी पढ़ा रही हूँ। आज मेरा मुख्य केंद्र बच्चों की शिक्षा है। मैं अब एक टीचर होकर कह सकती हूँ कि पढ़ाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। हम अपने बहुजन बच्चों को एक अच्छी और समझ की शिक्षा दे रहे हैं। एक ऐसी शिक्षा जो हमको नहीं मिली। मैं हमेशा कोशिश करुँगी कि मैं एक अच्छी टीचर बनूँ ताकि जो मेरे साथ मेरे स्कूल में हुआ… चाहे वो भेदभाव हो, सम्मान ना मिलना हो या अपनी बातों को सामने रखने की आज़ादी न मिलना हो, मैं नहीं चाहती कि इन सभी परिस्थितियों से मेरे बच्चों को गुज़रना पड़े।

स्कूल के बच्चे
मैं चाहूँगी कि वे ऐसे इंसान बनें जो पढ़ना-लिखना तो सीखें ही, साथ ही वे अपनी बातों को लोगों के सामने आसानी से रख पाएँ। खुद की इज्जत करें, सामने वाले की इज्जत करें। खुद के हक की व दूसरों के हक की लड़ाई लड़ें। मैं चाहती हूँ कि वे सोचने-समझने वाले व्यक्ति बनें। इसीलिए हमने जो बातें सीखी हम उन्हें अपनी क्लास में भी लाए। हमने बच्चों को बाबासाहब आंबेडकर व सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले की जीवनी और विचारों, संघर्षों को पढ़ाकर चर्चाएँ कीं। पारिवारिक व सामाजिक चुनौती से भरे मुश्किल के दौर में मेरे बच्चे ही उम्मीद की किरण की तरह हैं। एक बार जब बस्ती के लोगों ने हम कुछ टीचर्स को घेरकर फिर से वही सवाल-जवाब शुरू कर दिया था और सरस्वती पूजा करवाने से लेकर मेरे पहनावे पर टिप्पणियाँ हो रही थीं, जब बहसबाजी के बाद मैं स्कूल के अन्दर आई तो देखा कि पूरे समय बच्चे चुपचाप अन्दर बैठकर बहस को सुन रहे थे। कुछ ने मुझसे कहा कि मैडम आपसे हमने पुछा नहीं था इसीलिये नहीं आए मगर मन कर रहा था कि हम भी बाहर आकर उन लोगों को जवाब दें। एक बच्चे ने कहा कि वो लोग हमको सरस्वती पूजा करने को बोल रहे थे? हम उनको क्यों पूजें? उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? हम जैसे बच्चों को तो शिक्षा देने का काम सावित्रीबाई ने किया है, किसी सरस्वती ने नहीं। इस बात को सुनकर मेरी आँखों में आँसू आ गए और मुझे इस कविता की याद आई:
मेरे देश में
हज़ारों वर्षो से सरस्वती बाँट रही थी शिक्षा
फिर भी मेरी पीढियाँ रह गईं अशिक्षित
मेरे देश में
हज़ारों वर्षों से लक्ष्मी बाँट रही थी धन और वैभव
फिर भी मेरी पीढ़ियाँ रह गईं निर्धन
क्यों?
इस कविता के लेखक को मैं नहीं जानती। एक साथी ने मुझे भेजी थी और उनको भी लेखक की जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इस कविता को खुद के जीवन से एकदम जोड़कर देख पाई। क्योंकि वे कथित देवियाँ हमारी नहीं थीं इसलिए उन्होंने हमारे हिस्से की शिक्षा और धन दे दिया उनके ‘अपनों’ को। वे हमें छलती रहीं और हम उन्हें पूजते रहे। क्यों?
~~~
झरना साहू 1996 में मजदूरों द्वारा खुद बनाए और चलाए जा रहे एक स्कूल में पिछले छह वर्षों से पढ़ा रही हैं।
Magbo Marketplace New Invite System
- Discover the new invite system for Magbo Marketplace with advanced functionality and section access.
- Get your hands on the latest invitation codes including (8ZKX3KTXLK), (XZPZJWVYY0), and (4DO9PEC66T)
- Explore the newly opened “SEO-links” section and purchase a backlink for just $0.1.
- Enjoy the benefits of the updated and reusable invitation codes for Magbo Marketplace.
- magbo Invite codes: 8ZKX3KTXLK
MAI DUA KARTA HU KI AAP HAMESHA SALAMAT RAHE AUR AISE HE KAAM KARTE RAHE EDUCATION SE BADHKAR KUCH NAHI HAI
THANKYOU FOR SHARING
HUM LOG HAMESHA AAPKE SATH HAI AUR BACHHO KE SATH BHI
बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसे लोगो के सपोर्ट से ही हम ऐसे काम कर पाते हैं।
बच्चों को पढ़ाना ही काफ़ी नही बल्कि उन्हें शिक्षित करना भी जरूरी है
बहुत प्रभावशाली लेख। दिल से निकली आवाज। झरना एक समझदार टीचर लगती हैं, उन्हें अनेकों शुभकामनाएं। क्या उनसे सीधे बातचीत हो सकती है?
अगर आपके विद्यालय में बच्चों को संविधान की शिक्षा दी जाए और बच्चों को संविधान पढ़ाया जाए तो बच्चे कानून और लोगों से मजबूती से लड़ सकेंगे क्योंकि बच्चों को पता होगा की हमें क्या करना चाहिए कहां पर हमें लोगों से डटकर सामना करना चाहिए और संविधान के द्वारा बनाए गए नियम को साथ लेकर यह बच्चे और आगे बढ़ सकते हैं
नाम_ शुभम मौर्य
पता_ प्रयागराज
समाज सेवी
🙏जय भीम नमो बुद्धाय 🙏
आपके विद्यालय में बच्चों को बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को भी पढ़ाया जाए तो बच्चों को कानून के बारे में भी ज्ञान होगा और बच्चों को बाबा साहब के द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार लोगों से और कानून से डटकर सामना कर सकते हैं
शुक्रिया आपने अपना कीमती समय निकाल कर यह लेख पढ़ा।
अगर आप मुझसे सीधा बात करना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं।
jharnasahu87@gmail.com