
अरविंद शेष (Arvind Shesh)
 पिछले कुछ समय से लगातार यह मांग उठ रही थी कि अगर कोई सवर्ण पृष्ठभूमि का व्यक्ति जाति से अभिन्न समाज में बदलाव लाने की इच्छा रखता है तो उसे सबसे पहले ‘अपने समाज’ यानी अपने जाति-वर्ग को संबोधित करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जाति का समूचा ढांचा न केवल उच्च कही जाने वाली जातियों की मर्जी से संचालित है, बल्कि उनके हक में भी है। इसलिए पारंपरिक सवर्ण आमतौर पर जाति के ढांचे के बने रहने में ही ‘समाज का भला’ मानता है। ऐसे में अगर समाज की निचली कही जाने वाली जातियों की ओर से जाति के खिलाफ कुछ होता भी है तो उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि समाज आखिरकार राज से चलता है। राज एक सुगठित तंत्र के सहारे अपना काम करता है। और तंत्र पर आज देश की सत्तर साल की आजादी के बाद भी सवर्ण जातियों का प्रभुत्व या वर्चस्व है। तो जब तक राज की ओर से जाति व्यवस्था के खिलाफ एक ठोस बदलाव की बुनियाद पर कोई वास्तविक घोषणा नहीं होती है, तब तक जाति के खिलाफ लड़ने वाले निचली कही जाने वाली जातियों को कोई खास कामयाबी नहीं मिलेगी।
पिछले कुछ समय से लगातार यह मांग उठ रही थी कि अगर कोई सवर्ण पृष्ठभूमि का व्यक्ति जाति से अभिन्न समाज में बदलाव लाने की इच्छा रखता है तो उसे सबसे पहले ‘अपने समाज’ यानी अपने जाति-वर्ग को संबोधित करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जाति का समूचा ढांचा न केवल उच्च कही जाने वाली जातियों की मर्जी से संचालित है, बल्कि उनके हक में भी है। इसलिए पारंपरिक सवर्ण आमतौर पर जाति के ढांचे के बने रहने में ही ‘समाज का भला’ मानता है। ऐसे में अगर समाज की निचली कही जाने वाली जातियों की ओर से जाति के खिलाफ कुछ होता भी है तो उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि समाज आखिरकार राज से चलता है। राज एक सुगठित तंत्र के सहारे अपना काम करता है। और तंत्र पर आज देश की सत्तर साल की आजादी के बाद भी सवर्ण जातियों का प्रभुत्व या वर्चस्व है। तो जब तक राज की ओर से जाति व्यवस्था के खिलाफ एक ठोस बदलाव की बुनियाद पर कोई वास्तविक घोषणा नहीं होती है, तब तक जाति के खिलाफ लड़ने वाले निचली कही जाने वाली जातियों को कोई खास कामयाबी नहीं मिलेगी।
इसीलिए उच्च जातियों की पृष्ठभूमि वाले सक्षम लोगों से यह उम्मीद और मांग की जाती रही है कि वे अपने जाति-वर्गों को अगर बदल जाने और जाति की पहचान छोड़ कर जातिविहीन हो जाने के लिए तैयार कर लेते हैं तो जाति-आधारित समस्या का हल निकल सकता है।
तो क्या यह माना जाए कि अनुभव सिन्हा ने इस मांग की ‘संवेदना’ और ‘संवेदनशीलता’ का समझा और इसे ही ध्यान में रख कर ‘आर्टिकल 15’ फिल्म बनाई! यह संभावना इसलिए है कि ‘आर्टिकल 15’ को उसी श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसमें एक तरह से यह आईना मौजूद है, जिसमें अपना चेहरा देख कर उच्च कही जाने वाली जातियों में पैदा कुछ संवेदनशील लोगों के भीतर तोड़-फोड़ मच सकती है या कम से कम शर्म पैदा हो सकती है। हालांकि आज भी उच्च कही जाने वाली जातियों में पैदा पारंपरिक मानसिकता में जीने वाले लोग अगर इस फिल्म को देखें तो उनके भीतर तोड़-फोड़ मचाने के लिए फिल्म में कोई खास खुराक नहीं पेश की गई है।
यथास्थिति का रास्ता
लेकिन अगर कोई इसे दलित-वंचित जातियों-तबकों के मौजूदा राजनीतिक-सामाजिक और वैचारिक विमर्श की फिल्म मानता है तो यह खुद को महज एक वहम में रखने की बात होगी। कायदे से कहें तो यह फिल्म दलित-बहुजन के मौजूदा दौर के एसर्शन या दखल के बरक्स एक रूपक रचती है और संविधान के ‘आर्टिकल 15’ के कुछ प्रावधानों के तहत समानता स्थापित करने का संदेश देती है। लेकिन फिल्म के संदेश के मुताबिक वह समानता क्या है? किसी व्यक्ति से जाति या अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो। फिल्म की कहानी संविधान के अनुच्छेद को तंत्र यानी पुलिस महकमे के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि वह भेदभाव खत्म हो। लेकिन यह तब मुमकिन है जब कोई ऐसा ईमानदार और वरिष्ठ स्तर का पुलिस अफसर हो जो जाति के दड़बे में नहीं पला-बढ़ा हो और जाति के जहर को देख कर द्रवित हो जाता हो, उसके भीतर दया का भाव उमड़ता हो। वह एक ‘पोजिशन’ हो, सामाजिक और प्रशासनिक भी, जो संविधान में दर्ज किसी नियम को लागू करने का जिम्मा उठा सकता हो। इस नियम के सहारे वह भेदभाव नहीं होने देने की बात कर सकता है, लेकिन भेदभाव की मूल वजहों पर चोट करना उसके बस में नहीं है।
बहरहाल, अपनी सीमा में वह सामूहिक बलात्कार की एक घटना के सिरे से समाज में पसरे जाति के जाल को देखने की कोशिश करता है और ज्यादा से ज्यादा ‘सामाजिक समरसता’ के सिद्धांत तक पहुंच पाता है, जहां फिल्म के अंतिम दृश्य में सड़क किनारे एक छोटी दुकान लगाए बैठी एक वृद्ध महिला के हाथ की बनी रोटी वह अपनी पूरी टीम को खिलाता है और पूछता है- ‘कौन जात हो अम्मा..!’ और जवाब में वहीं से गुजरती एक ट्रक की पीं-पीं का शोर गूंजता है। यानी जाति का सवाल खत्म..! क्या कह सकते हैं कि यानी जाति का सवाल दफ्न…?
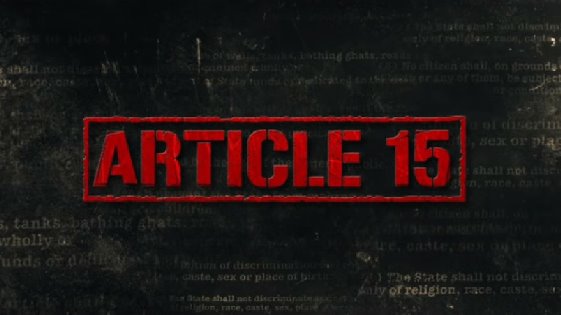
सुधार का सरोकार
इसके बावजूद फिल्म जाति के सवाल से जूझती हुई दिखती है, लेकिन टकराती नहीं है। समाज का जो ढांचा चला आ रहा है, उसमें कानून के खिलाफ कुछ न हो। कानून और संविधान समानता का अधिकार देता है, लेकिन समाज कुछ और देता है। फिल्म में अंशु नहारिया कहता है- ‘हम (दलितों को) जो देते हैं, वही औकात है!’ सदियों बाद कोई अयान रंजन आएगा, अपने ‘पोजिशन’ के जरिए किसी एकाध घटना में संविधान में दर्ज अधिकार ‘दिलाने’ की कोशिश करेगा, लेकिन ‘समाज’ जो देता है, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी?
हालांकि फिल्म इस सवाल से टकराने का दावा भी नहीं करती। खुद अनुभव सिन्हा का मानना है कि तंत्र में अगर ब्राह्मण बैठा है तो वही सुधारने की कोशिश करे। दिक्कत वहां है, जहां देश और विदेश के आभिजात्य आबोहवा में पला-बढ़ा अयान रंजन वह ब्राह्मण है, जो सुधारने का बीड़ा उठाएगा। फिल्म के बाकी पात्र खालिस सच के करीब रखने कोशिश के बीच अयान रंजन या तो एक बनावटी पात्र लगता है या फिर किसी ‘सिंघम’ टाइप हीरो, जिसके सामने कोई भी मुश्किल जीरो हो जाती है।
हीरो को पता चलता है कि बलात्कार करके मार डाली गई दो दलित लड़कियों के साथ यह सब सिर्फ इसलिए हुआ कि उन्होंने दिहाड़ी में महज तीन रुपए बढ़ाने के लिए कहा था। ‘सिर्फ तीन रुपए… यानी जो मिनरल वाटर आप पी रहे हैं, उसका एक-या दो घूंट..!’ लेकिन सच क्या है? सच यह है कि जिन दो लड़कियों से बलात्कार और उनकी हत्या हुई, उनके साथ केवल तीन रुपए के लिए नहीं, दलित होने के नाते वैसा हुआ। सवर्ण पृष्ठभूमि के परिवार इस समस्या से लगभग मुक्त हैं।
विरोधाभासों का घुलना-मिलना
खैर, यह फिल्म अपनी इसी सीमा के साथ अंत तक चलती है। मारी गई लड़कियों के पिता कहते हैं कि उनको कुछ दिन रख लेते, मार काहे दिए! सालों पहले प्रेमचंद की कहानी ‘कफन’ पर ये सवाल खड़े हो चुके हैं कि दलित पात्रों की हीनता और उनका अमानवीयकरण कितना सच है, कितना जायज था और एक लेखकीय जवाबदेही क्या होती है! सवाल है कि एक फिल्म में समांतर स्तर पर ‘जय भीम’ के नारे के साथ ‘भीम संघर्ष सेना’ और जान बचने की कीमत पर अपनी बेटी को कुछ दिन रख लिए जाने की त्रासदी को सहजता से स्वीकार किया जाना कैसे मुमकिन हुआ? खासतौर पर तब जब ‘भीम संघर्ष सेना’ के सबसे मुख्य नेता ‘निषाद’ की साथी गौरा उन लड़कियों के पिता के सीधे-सीधे साथ थी, रोजमर्रा के तौर पर। और खुद उसकी बहन भी मारी गई लड़कियों के साथ ही गायब हो गई थी। वह गौरा, जो फिल्म को एक शानदार क्रांतिकारी और परिपक्व शुरुआत देती है- ‘कहब त लाग जाई धक से…!’ अगर ‘भीम संघर्ष सेना’ का रूपक लिया ही गया है तो उसके नेता उस ‘निषाद’ की प्रेमिका क्या इतना कमजोर और दयनीय पात्र हो सकती थी जो समूची व्यवस्था के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का ‘थोड़ा ज्यादा ही पढ़-लिख गया’ क्रांतिकारी था?

लेकिन जब ‘निषाद’ का ही चरित्र नहीं गढ़ा जा सका, तो उसकी प्रेमिका गौरा को कैसा बनाया जा सकता था! ‘भीम सेना’ के नेता चंद्रशेखर और रोहित वेमुला की छवि उतारने के क्रम में ‘निषाद’ को ऐसा बना दिया गया कि बागी की छवि झलकने से आगे प्रेमिका की गोद में सिमट कर रोने और उसके बाद मुठभेड़ में मार डाले जाने से ज्यादा उसके हिस्से कुछ आया ही नहीं। जो लोग रोजमर्रा के राजनीतिक जेनरल नॉलेज से रूबरू हैं, वही ‘निषाद’ को या तो ‘भीम सेना’ से जोड़ कर देख पाते हैं। लेकिन उनके सामने ‘निषाद’ की भूमिका पर कई सवाल उठते हैं। ‘आर्टिकल 15’ लागू करने की कोशिश करते अयान रंजन के टास्क में ‘निषाद’ का उपयोग सिर्फ इतना था कि वह एससी कर्मचारियों की हड़ताल से पैदा बजबजाते नालों की सफाई के लिए कुछ कर्मचारियों को काम पर आने की इजाजत दे दे।
तल्ख सवालों का सामना
उदारवादी अयान रंजन जातियों से जुड़ी तकलीफ पर द्रवित होता है, लेकिन गंदगी से बजबजाते नाले-नालियों और गंदगी की सफाई के लिए उसे समाज में निर्धारित या तयशुदा लोग ही चाहिए। ब्राह्मण-दलित एकता रैली के विरोध पर टिका निषाद इस बात पर राजी होता है कि उसकी प्रेमिका गौरा की बहन ‘पूजा के मिल जाने की उम्मीद है’। इसके बावजूद यह कहा जा सकता है कि फिल्म के इस दृश्य में कुछ तल्ख सवालों का सामना करने की कोशिश की गई है। मगर इन सवालों के बाद अगले ही दृश्य में गंदगी से बजबजाते नाले में डुबकी लगा कर एक इंसान सफाई करता नजर आता है, केस और पूजा को खोजने का काम आगे बढ़ता है।
इसके बाद एक आइपीएस के इलाके में बिना उसे खबर किए किसकी पुलिस कहां से आती है, ‘निषाद’ को उठा कर ले जाती है और फर्जी मुठभेड़ में मार डालती है। क्या यही ‘निषाद’ की नियति थी/है? तीन रुपए ज्यादा मांगा तो दोनों लड़़कियों का बलात्कार और हत्या! दलितों के हकों के लिए आवाज उठाई तो ‘निषाद’ की हत्या! ब्राह्मण-दलित रैली के विरोध में खड़े हुए तो हिंसा करने का आरोप… और इसके बाद क्या होता है, क्या यह किसी से छिपा है! दूसरी ओर, किसी भी रास्ते जीता, महंथ जीता… ‘ब्राह्मण-दलित एकता’ के नारे के साथ! आखिर फिल्म की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्पेशल थैक्स मिला है!
खैर, भारत में ‘जन’ के संदर्भ ‘वैष्णव जन’ से लेकर वामपंथ के जनवाद के ‘जन’ तक रहे हैं। बिहार के ग्रामीण इलाकों में खेत या किसी काम में मजदूरी करने वालों को भी ‘जन’ कहते हैं। और भी आशय हो सकते हैं। फिल्म का इंटरवल ‘आर्टिकल 15’ का पर्चा दीवारों पर लगाने के दृश्य के बैकग्राउंड में बजते ‘वंदे मातरम्’ के साथ और फिल्म का अंत बैकग्राउंड में बजते ‘वैष्णव जन तो तैणे कहिए..’ के धुन के साथ! तो फिल्म के सबसे मशहूर संवाद ‘कभी हम हरिजन हुए, कभी बहुजन हुए, बस जन नहीं हो सके’ के जरिए ‘निषाद’ किस ‘जन’ के सपने की बात करता है? चूंकि आज का ‘बहुजन’ गांधी के ‘हरिजन’ के बरक्स है, इसलिए जब ‘हरिजन’ के साथ-साथ उसी सुर में ‘बहुजन’ को भी खारिज किया जाता है तो यह जानने की इच्छा लाजिमी है।
‘आर्टिकल 15’ लागू करने की छाया के साथ चलती कहानी में यही सामने आता है कि दलित-वंचित तबकों की ओर से अगर कोई भी आवाज उठेगी तो उसका हश्र उन दोनों लड़कियों से लेकर ‘निषाद’ जैसा ही होगा! इसके बावजूद कि ‘निषाद’ सचेतन ‘अपने लोगों’ को हिंसा नहीं करने की हिदायत देता है क्योंकि वे और ज्यादा मारेंगे। यानी एक सीमा-रेखा तय है। इसे स्वीकार करने पर जिंदा रहना संभव हो सकता है, इस रेखा पर पांव रख कर खड़ा हो जाने का मतलब उस आवाज का हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाना! क्या इस नियति के बरक्स कोई विकल्प नहीं है, ‘सामाजिक समरसता’ से इतर?
नाम की परतों तले
यह ‘निषाद’ कौन है? पूरी फिल्म देखने के बावजूद यह पता नहीं चला कि कहीं भी इस चरित्र का ‘निषाद’ के सिवा कुछ और भी नाम है या नहीं! मल्लाह या निषाद एक जाति होती है, ज्यादा से ज्यादा किसी नाम का टाइटिल। लेकिन समूची फिल्म में ‘निषाद’ केवल इसी शब्द के साथ मौजूद है। गनीमत है कि एक अन्य दलित पात्र ‘जाटव जी’ का नाम अयान रंजन के साथ परिचय के क्रम में सिर्फ एक बार शुरुआती तौर पर आता है- किसन जाटव। वरना पूरी फिल्म में वह चरित्र ‘जाटव जी’ है, जबकि उसके साथ विलेन के पात्र के रूप में कोई ब्रह्मदत्त जी है तो कोई निहाल सिंह है तो कोई मयंक है। सबके नाम से पुकारा जाता है, किसन जाटव शुरू से अंत तक सिर्फ ‘जाटव जी’ रह जाते हैं। ‘जाटव’ भी ‘निषाद’ की तरह एक जाति का नाम है और ज्यादा से ज्यादा टाइटिल।

जाति के पहलू पर कहानी ऐसी उलझी हुई है कि कई बार ऊब महसूस होती है। सीबीआई अफसर पणिक्कर आइपीएस अयान रंजन से कहता है कि आपने अपने सहयोगियों से जाति पूछी। …ये एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत क्राइम है। केवल फिल्म में मनोरंजन के लिए ये संवाद डाले गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन चूंकि यह फिल्म सामाजिक और खासतौर पर जाति के सवालों से मुठभेड़ करने का दावा करती है इसलिए हैरानी होती है। यह किसी भी मामूली जागरूक व्यक्ति को भी पता होगा कि किसी की जाति पूछना एससी-एसटी एक्ट के तहत क्राइम नहीं है, उसे जाति के आधार पर अपमानित करना या उससे भेदभाव करना क्राइम जरूर है। हालांकि सीबीआई अफसर पणिक्कर से ही संवाद फिल्म का दूसरा मौका है, जब एक ब्राह्मण पुलिस अफसर जाति को आईने के तौर पर सामने रखने की कोशिश करता है, कुछ तल्खी के साथ।
एक आदर्श हरिजन ‘जाटव जी’
‘ये लोग ऐसे चले आते हैं’… ‘इन लोगों के यहां ऐसा ही होता रहता है…’ ‘ऐसी बस्ती में रहोगे, जहां हगोगे, वहीं खाओगे, वहीं जानवर छिले पड़े हैं…! साला तुम अपना जीवन सुधारोगे नहीं, हम बन जाएं राजा राम मोहन राय..!’ ये संवाद बोलने वाले मुख्य पात्र ‘जाटव जी’ हैं, जो खुद दलित पृष्ठभूमि से हैं। क्या हम गौर कर सकते हैं कि पिछले कुछ समय से जाति के आधार पर आरक्षण को खत्म करने की वकालत करने वाले नेताओं में जो कुछ लोग खुल कर सामने आए, वे आमतौर पर दलित पृष्ठभूमि से हैं? जब जाटव जी जैसा कोई ‘इनसाइडर’ अपने समाज के बारे में इस तरह की ‘हकीकत’ का बयान करता है तब तमाम ‘आउटसाइडरों’ के सामने कुछ और सोचने का क्या विकल्प रह जाता है?
ये ‘जाटव जी’ शुरुआती दृश्यों में अपने नए ब्राह्मण अफसर के सामने से अपनी थाली हटा लेते हैं कि कहीं वह उनकी थाली में से कुछ लेकर खा न ले और कहीं उसे छूत न लग जाए! इसके अलावा, उसी अफसर के मुंह से गु्स्से में निकले अंग्रेजी वाक्य को नहीं समझ पाने का मजाक भी ‘जाटव जी’ को बनना था, वहीं आसपास मौजूद अन्य सवर्ण या दूसरे पुलिसकर्मियों या अफसरों को नहीं।
बहरहाल, पूरी फिल्म में ‘हरिजन’ बने रहे जाटव जी एक मौके पर बहुजन या दलित बनते हैं, जब हवालात में भेजे जाते समय ब्रह्मदत्त सिंह के हमले के जवाब में उसे एक थप्पड़ लगा कहते हैं कि कब तक झाड़ू लगवाइएगा। लेकिन तत्काल सिर पर से टोपी उतार कर फिर से शायद अपनी हैसियत में आ जाते हैं। यही ‘जाटव जी’ किसी की जाति बताते समय जिस सहजता से दपदपाते रहते हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनके पास जाति का कोई भी दंश मौजूद नहीं है। इसे ‘अपने’ समाज के प्रति ‘कृतघ्नता-भाव’ के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यही ‘सोशल पोजिशनिंग’ की वह भूख है, खुद को ‘नीच’ कहे जाने वालों से अलगाने की भूख है, जिसके मनोविज्ञान को समझना इतना आसान नहीं है!
वर्चस्व की लगाम
बाकी ब्रह्मदत्त के मुंह से जब ये सुवचन निकलते हैं कि सत्ता में रहते हैं तो मूर्तियां बनवाते रहते हैं और सत्ता से बाहर होते हैं तो दलित बन जाते हैं या फिर ‘आप किसको वोट देते हैं… आप किसको वोट देते हैं…’ के मौके पर बताया जाता है कि दलित राजनीति की दिशा कौन तय करेगा! दलित राजनीति अपनी गलतियों से नुकसान उठाए तब भी यही तय करेंगे कि उस पर कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए।
दलित समुदाय के ही ‘पासी’ जाति के तीन लड़कों को सार्वजनिक रूप से पीटने के दृश्य से ‘उना कांड’ की बर्बरता को उभारने की कोशिश की गई है, लेकिन वजह बदल गई। उना में आजीविका के साधन के तौर पर मरी गायों का चमड़ा उतारने के एवज उन चार दलित युवकों को उसी तरह पीटा गया था, यहां मंदिर में खाना खाने के आरोप में पीटा गया। फिल्म है तो इससे क्या अलग उम्मीद की जाएगी, लेकिन जब कोई फिल्म सरोकार निबाहने का दावा करती है तब सवाल बनते हैं।
इसके बावजूद इस फिल्म का स्वागत इसलिए होना चाहिए कि भले ही यह सवर्ण लोकेशन से बनी फिल्म है, लेकिन जाति और उसकी हकीकतों पर बात करती है। जाति इस समाज की सबसे बड़ी समस्या है और इस पर बात करने भर से व्यवस्थावादियों को अपनी सत्ता जाने का डर सताने लगता रहा है। इतना तय है कि जाति पर जब बेधड़क-बेहिचक बातचीत होने लगेगी तब उसका सिरा अंतिम रूप से दलित-वंचित जातियों-तबकों के हक में जाएगा।
प्रतिरोध के बरक्स परनिर्भरता
बहरहाल, जुलाई, 2015 में ‘गुड्डू रंगीला’, जून 2016 में ‘कबाली’ और जुलाई 2018 में ‘काला’ फिल्म के बाद जब ‘आर्टिकल 15’ आती है तो मन में यह उथल-पुथल तो होगी कि क्या यह उन फिल्मों से आगे की फिल्म है! लेकिन यह ‘गुड्डू रंगीला’, ‘कबाली’ और ‘काला’ की कड़ी की फिल्म नहीं है, क्योंकि ये फिल्में सोशल जस्टिस के लिए संघर्ष और दखल या एसर्शन की फिल्में हैं। जबकि ‘आर्टिकल 15’ संविधान, सत्ता और तंत्र पर कब्जा किए बैठे सवर्ण वर्चस्व के भरोसे इंसाफ की उम्मीद करते, इंसाफ की भीख मांगते दलितों की। बगावत की एक छौंक जो ‘निषाद’ के जरिए लगाने की कोशिश है भी, उसे भी फर्जी मुठभेड़ में ही सही, मार डाला जाना है।
कायदे से कहें तो यह ‘पिंक’ फॉरमेट की फिल्म है। जिस तरह ‘पीकू’, ‘क्वीन’ और ‘पार्च्ड’ या फिर ‘अनारकली ऑफ़ आरा’ में अपनी लड़ाई खुद लड़ती स्त्रियों की कहानी के बाद ‘पिंक’ आई, जिसमें जान लेने वाला भी पुरुष और जान बचाने वाला भी पुरुष ही था, उसी तरह ‘गुड्डू रंगीला’, ‘कबाली’ और ‘काला’ में ताकतवर बहुजन एसर्शन है, अपनी लड़ाई खुद लड़ते हाशिये के ये तबके हैं, वहीं ‘आर्टिकल 15’ है जिसमें दलितों-वंचितों पर अत्याचार और उनके लिए लड़ी जाने वाली न्याय और करुणा की कहानी है, लेकिन अत्याचार करने वाला भी सवर्ण और बचाने वाला भी सवर्ण! इसलिए ‘आर्टिकल 15’ आज के दलित-बहुजन विमर्श की फिल्म नहीं है। यह सवर्णों को आईना दिखाने वाली फिल्म है, उनके भीतर संवेदना जगाने और सभ्य बनाने की कोशिश करने वाली फिल्म है। अब देखने की बात यह होगी कि इस फिल्म से पैदा कड़वाहट को सवर्ण समुदाय के लोग कैसे और किस हद तक पचा पाते हैं, उनका किस स्तर तक कायाकल्प हो पाता है!
~~~
अरविन्द शेष जाने माने पत्रकार हैं. उनसे arvindshesh@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है.
तस्वीरें गूगल से साभार
Magbo Marketplace New Invite System
- Discover the new invite system for Magbo Marketplace with advanced functionality and section access.
- Get your hands on the latest invitation codes including (8ZKX3KTXLK), (XZPZJWVYY0), and (4DO9PEC66T)
- Explore the newly opened “SEO-links” section and purchase a backlink for just $0.1.
- Enjoy the benefits of the updated and reusable invitation codes for Magbo Marketplace.
- magbo Invite codes: 8ZKX3KTXLK